12. काव्य-बोध (काव्य की परिभाषा एवं भेद, रस, अलंकार, छन्द)
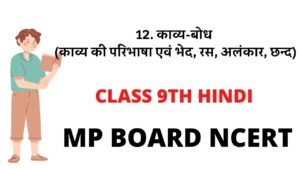
प्रश्न 8. खण्डकाव्य किसे कहते हैं ? हिन्दी के प्रसिद्ध खण्डकाव्यों के नाम लिखिए।
अथवा
किन्हीं दो खण्डकाव्यों के नाम लिखिए।
उत्तर-खण्डकाव्य-खण्डकाव्य वह रचना है जिसमें जीवन का कोई एक भाग, एक घटना अथवा एक चरित्र का चित्रण होता है। खण्डकाव्य अपने आप में एक पूर्ण रचना होती है। सम्पूर्ण रचना एक ही छन्द में पूर्ण होती है।
हिन्दी के कुछ प्रसिद्ध खण्डकाव्य-पंचवटी, जयद्ध-वध, नहुष, सुदामाचरित, पथिक, हल्दीघाटी
इत्यादि।
प्रश्न 9. महाकाव्य और खण्डकाव्य में कोई दो अन्तर लिखकर एक-एक रचना तथा रचनाकार का नाम लिखिए।
अथवा
महाकाव्य एवं खण्डकाव्य में कोई तीन अन्तर लिखिए।
उत्तर-अन्तर
-(1) महाकाव्य में जीवन की विशद् व्याख्या होती है, जबकि खण्डकाव्य में जीवन का कोई एक भाग, एक घटना अथवा एक चरित्र का चित्रण होता है।
(2) महाकाव्य सर्गबद्ध होता है। इसमें कम-से-कम आठ सर्ग होते हैं, जबकि खण्डकाव्य अपने आप में एक पूर्ण रचना होती है। (3) पात्रों, घटनाओं आदि की संख्या महाकाव्य में अधिक होती है, जबकि खण्डकाव्य में इनकी संख्या कम होती है।
रचनाएँ एवं रचनाकार- महाकाव्य-रामचरितमानस (तुलसीदास)।
खण्डकाव्य-सुदामाचरित (नरोत्तमदास)।
प्रश्न 10. मुक्तक काव्य किसे कहते हैं ? इसके प्रकार बताइए।
अथवा
मुक्तक काव्य किसे कहते हैं ? उदाहरण सहित लिखिए।
उत्तर-मुक्तक काव्य-मुक्तक काव्य में एक अनुभूति, एक भाव और एक ही कल्पना का चित्रण होता है। मुक्तक काव्य की भाषा सरल एवं स्पष्ट होती है। वर्ण्य विषय अपने आप में पूर्ण होता है। इसका
प्रत्येक छन्द स्वतन्त्र होता है।
उदाहरण-
रहिमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय।
टूटे से फिर ना जुड़े, जुडै गाँठ पढ़ जाय॥
मुक्तक काव्य दो प्रकार के होते हैं-(1) पाठ्य मुक्तक, (2) गेय मुक्तक।
पाठ्य मुक्तक-पाट्य मुक्तक में विषय की प्रधानता होती है। प्रसंगानुसार भावानुभूति व कल्पना का चित्रण होता है तथा किसी विचार या रीति का भी चित्रण होता है।
गेय मुक्तक-इसे गीति या प्रगीति काव्य भी कहते हैं।
इसमें-
(1) भाव-प्रवणता,
(2) सौन्दर्य-बोध,
(3) अभिव्यक्ति की संक्षिप्तता,
(4) संगीतात्मकता,
(5) लयात्मकता की प्रधानता होती है।
प्रश्न 1, रस किसे कहते हैं ? इसकी परिभाषा लिखिए। स्थायी भाव और संचारी भाव अन्तर
उत्तर- रस को काव्य की आत्मा बताया गया है। जिस तरह आत्मा के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं होता, उसी तरा रस के बिना काव्य भी निर्जीव माना गया है। “रसात्मकम वावयम कायम” अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है।
यदि काव्य की तुलना मनुष्य से की जाए तो शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर, अलंकारों को आभूषण, कन्दों को उसका बाहा परिधान तथा रस को आत्मा कह सकते हैं। काय रस का अर्थ आनन्द बताया गया है। साहित्यशास्त्र में ‘रस’ का अर्थ अलौकिक या लोकोत्तर आनन्द होता है। अत: काव्य के पढ़ने, सुनने अथवा
उसका अभिनय देखने में पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनन्द मिलता है, वही काव्य में रस कहलाता है। बदल जाते हैं।
स्थायी भाव-ये भाव मनुष्य हृदय में सुप्त अवस्था में रहते हैं परन्न अवसर पाकर पुष्ट होकर रस में
पुष्ट करके नष्ट हो जाते हैं।
संचारी भाव-आश्रय के मन में अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये स्थायी भाव को
प्रश्न 2. रस के अंगों (रस को आस्वाद योग्य बनाने में सहायक अवयव) के नाम लिखिए।
उत्तर-रस के चार अंग होते हैं-(1) स्थायीभाव, (2) विभाव, (3) अनुभाव, (4) संचारीभाव।
विभाव के दो भेद होते हैं-(1) आलम्बन, (2) उद्दीपन।
आलम्बन भी दो प्रकार होता है-(1) आश्रय, (2) विषय।
प्रश्न 3. रस किसे कहते हैं ? रस के प्रमुख अंगों के नाम लिखिए।
उत्तर-प्रश्न । व2 का उत्तर देखें।
प्रश्न 4. रस के भेद बताइए तथा प्रत्येक रस के स्थायी भाव स्पष्ट कीजिए।
उत्तर- रस
स्थायी भाव
1. शृंगार
रति
2. हास्य
हास
3. करुण
शोक
4.रौद्र
क्रोध
5. वीभत्स
जुगुप्सा
6. भयानक
भय
7. अद्भुत
विस्मय
8. वीर-
उत्साह
9.शान्त
निर्वेद
विशेष-आचार्य भरत ने नाटक में आठ रस माने हैं। परवर्ती आचार्यों ने शान्त रस को अतिरिक्त स्वीकृति देकर कुल नौ रस निश्चित कर दिए। काव्य में महाकवि सूरदास ने वात्सल्य प्रधान मधुर पदों की रचना की तो एक अन्य रस-‘वात्सल्य रस’ की भी स्थापना हो गई। आजकल भक्ति को भी रस रूप में स्वीकृति दिये जाने का आग्रह चल रहा है।
प्रश्न 5. रस के कोई पाँच प्रकार व उनके स्थायी भाव लिखिए।
उत्तर-प्रश्न 1 का उत्तर देखें।
प्रश्न 6. शृंगार रस की परिभाषा, भेद लिखिए और उदाहरण दीजिए।
उत्तर-शृंगार रस की निष्पत्ति रति’ स्थायी भाव के संयोग से होती है। इसके दो भेद हैं-(1) संयोग
शृंगार, (2) वियोग शृंगार।
संयोग शृंगार रस में नायक-नायिका के संयोग (मिलन) की स्थिति का वर्णन होता है।
उदाहरण-
“बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय।
सौंह करें’, भौहनि हँसै, दैन कहे नटि जाय ।।”
वियोग शृंगार रस में नायक-नायिका में बिछुड़ने का तथा दूर देश में रहने की स्थिति का वर्णन, वियोग
शृंगार की व्यंजना करता है-
उदाहरण-
“आँखों में प्रियमूर्ति थी, भूले थे सब भोग।
हुआ योग से भी अधिक, उसका विषम वियोग।”
प्रश्न 7. हास्य रस की परिभाषा सोदाहरण लिखिए।
उत्तर-हास्य रस-परिभाषा-किसी व्यक्ति के विकृत वेश, आकृति तथा वाणी आदि को देख व सुनकर हँसी उत्पन्न हो उठती है, वैसा ही वहाँ का वर्णन होता है, तो वहाँ हास्य रस की निष्पत्ति होती है।
उदाहरण-
“जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सजधज कर।
मन करता धक्का दे दूल्हे को, जा बैतूं घोड़े पर।
सपने में ही मुझको अपनी, शादी होती दिखती है।
वरमाला ले दुल्हन बढ़ती, बस नींद तभी खुल जाती है।”
प्रश्न 8. करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए।
उत्तर-करुण रस-परिभाषा-प्रिय वस्तु के विनाश अथवा अनिष्ट के होने से चित्त में जाग्रत शोक
भाव करुण रस को निष्पन्न करता है।
उदाहरण-
“अभी तो मुकुट बँधा था माथ,
हुए कल ही हल्दी के हाथ,
खुले भी न थे लाज के बोल,
खिले भी न चुम्बन-शून्य कपोल,
हाय ! रुक गया यहीं संसार,
बना सिंदूर अंगार॥”
प्रश्न 9.रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए।
रौद्र रस-परिभाषा-जब क्रोध नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट हुआ रस दशा को प्राप्त होता है, तो वहाँ रौद्र रस की निष्पत्ति होती है।
उदाहरण-
सुनत लखन के वचन कठोरा।
परसु सुधारि धरेउ कर घोरा॥
अब जनि देउ दोष मोहि लोगू।
कटु वादी बालक वध जोगू॥
प्रश्न 10. वीर रस की परिभाषा लिखिए और उदाहरण भी दीजिए।
अथवा
वीर रस की परिभाषा देकर एक उदाहरण दीजिए।
उत्तर-वीर रस-परिभाषा-वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। इस रस की निष्पत्ति ओजस्वी
वीर घोषणाओं या वीर गीतों को सुनकर अथवा उत्साह बढ़ाने वाले कार्यकलापों को देखने से होती है।
उदाहरण
काव्य-बोध (काव्य की परिभाषा एवं घेद, रस, अलंकार, छन्द)
वह खून कहो किस मतलय का,
जिसमें उबाल का नाप नहीं।
वह खून कहो किस मतलब का,
जिसमें जीवन की रवानी नहीं।
प्रश्न 1. भयानक रस की परिभाषा, उदाहरण सहित लिखिए।
उदाहरण-
उत्तर-भयानक रस-परिभाषा-भयानक रस का स्थायी भाव भय’ है। प्रकृति के डरावने दृश्यो,
अशा बलवान् शत्रु के प्राणनाशक बोलों को सुनकर भय को उत्पत्ति होने पर भयानक रस को निष्पत्ति होती है।
‘हाहाकार हुआ क्रन्दन मय, कठिन बड़ होते थे चूर।
हुए दिगन्त बधिर भीषण रव बार-बार होता था कूर ॥
अलंकार
प्रश्न 1. अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा इसके भेद बताइए।
उत्तर-अलंकार से तात्पर्य है-श्रृंगार करना या सजाना या आभूषित करना। जिस तरह एक नारी आभूषणों से अपने शरीर की सज्जा करती है, उसी तरह अलंकार वे तत्व हैं जिनसे काव्य की शोभा बढ़ती है। आचार्य विश्वनाथ के शब्दों में, “अलंकार शब्द-अर्थ-स्वरूप काव्य के अस्थिर धर्म है और भावों और रसों का उत्कर्ष
करते हुए वैसे ही काव्य की शोभा बढ़ाते हैं; जैसे हार आदि आभूषण नारी को सुन्दरता में चार चाँद लगा देते हैं।”
अलंकार के भेद तीन होते हैं-
(1) शब्दालंकार, (2) अर्थालंकार, (3) उभयालंकार।
(1) शब्दालंकार-शब्द विशेष के चमत्कार द्वारा जो अलंकार कविता का सौन्दर्य बढ़ायें, वे शब्दालंकार
होते हैं।
(2) अलंकार-काव्य में जहाँ अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करते हैं, वे अर्थालंकार कहलाते हैं।
(3) उभयालंकार-शब्द एवं अर्थ दोनों में चमत्कार पैदा करके काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, वे उभयालंकार
होते हैं।
प्रश्न 2. शब्दालंकार के भेद बताइए और प्रत्येक का नाम लिखिए।
उत्तर-शब्दालंकार के प्रमुख तीन भेद है-(1) अनुप्तास, (2) यमक, (3) श्लेष।
प्रश्न 3. अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, उदाहरण सहित लिखिए।
उत्तर-अनुप्रास-परिभाषा-जिस काव्य रचना में व्यंजन वर्ण को दो या दो से अधिक बार आवृत्ति
होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है।
“तरनि तनूजा तट तमाल, तरुवर बहु छाए।”
उदाहरण-
यहाँ त वर्ण की आवृत्ति की गई है, अतः अनुप्रास अलंकार है।
प्रश्न 4. यमक अलंकार की परिभाषा दीजिए तथा उदाहरण लिखिए।
उत्तर-यमक-परिभाषा-यमक अलंकार में एक शब्द बार-बार आए, किन्तु उसका अर्थ हर बार अलग-अलग हो, तो वहाँ यमक अलंकार होता है।
उदाहरण-
‘माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर।
कर का मनका डारि के, मन का मनका फेरि॥’
यहाँ मनका शब्द के दो अर्थ है-पहले मनका (मोती), दूसरे मन का अर्थात् ‘हृदय का’ है।
प्रश्न 5. श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए।
उत्तर-श्लेष अलंकार-परिभाषा-श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं।
ब्दाहरण- चिरजीवी जोरी जुरै क्यों न सनेह गंभीर।
को घटि ये वृषभानुजा वे हलघर के वीर ॥
वृषभानुजा – वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा। वृषभ की अनुजा = गाय। हलधर = कृष्ण के भाई
बलराम। हलधर- हल को धारण करने वाला बैल।
प्रश्न 6, अर्थालंकार के भेद बताइए और प्रत्येक का नाम लिखिए।
उत्तर-अर्थालंकार के तीन भेद होते हैं-(1) उपमा, (2) रूपक, (3) उत्प्रेक्षा।
प्रश्न 7. उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके अंग भी बताइए।
उत्तर-उपमा अलंकार-परिभाषा-जहाँ एक वस्तु अथवा प्राणी की तुलना अत्यन्त सादृश्य के कारण प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, तब वहाँ उपमा अलंकार होता है।
उदाहरण-
“सिंधु सा विस्तृत है अथाह,
एक निर्वासित का उत्साह ।।
उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं-
(1) उपमेय-जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है।
(ii) उपमान-जिस व्यक्ति या वस्तु से समानता की जाती है।
(ii) साधारण धर्म-वह गुण या धर्म जिसकी तुलना की जाती है।
(iv) वाचक शब्द-वह शब्द जो रूप-रंग, गुण और धर्म की समानता दर्शाता है; जैसे-सा, सी, सम,
समान आदि।
प्रश्न 8. रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण दीजिए।
उत्तर-रूपक अलंकार-परिभाषा-काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है, वहाँ रूपक
अलंकार होता है। इसमें वाचक शब्द का लोप होता है।
उदाहरण-
“चरण-सरोज पखारन लागा।”
प्रश्न 9. उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए।
उत्तर-उत्प्रेक्षा अलंकार-परिभाषा-काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान की सम्भावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जनु, जानो, मानो, मानहुँ आदि वाचक शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान हैं।
उदाहरण- “जनु, अशोक अंगार दीन्ह मुद्रिका डारि तब।”
“मानो, झूम रहे हैं, तरु भी मंद पवन के झोंकों से।”
प्रश्न 10. यमक और श्लेष अलंकार में उदाहरण सहित अन्तर स्पष्ट कीजिए।
उत्तर-यमक अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति अनेक बार होती है परन्तु उसके अर्थ में भिन्नता होती है। जबकि श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के दो या उससे अधिक अर्थ होते हैं। उदाहरण-
(1) करका मनका डारिके, मन का मनका फेरि । (यमक)
(2) को घटि ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। (श्लेष)
प्रश्न 11. अनुप्रास’ तथा ‘यमक’ अलंकार में भेद स्पष्ट करो।
उत्तर-अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है जबकि यमक अलंकार में भिन्न-भिन्न अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग दो अथवा दो से अधिक बार होता है।
उदाहरण-(अनुप्रास)-रघुपति राघव राजाराम-पतित पावन सीता राम।
यहाँ ‘र’ वर्ण एवं ‘प’ वर्ण की आवृत्ति है।
उदाहरण-(यमक)-कनक-कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाय।
या खाए बौराय जग, वा पाए बौराय। ‘कनक’ दो बार प्रयुक्त है, इसमें एक का अर्थ धतूरा’ तथा दूसरे का अर्थ स्वर्ण (सोना) है।
प्रश्न 1. छन्द की परिभाषा बताइए एवं उदाहरण लिखिए।
अथवा
छन्द किसे कहते हैं?
काव्य-बोध (काव्य की परिभाषा एवं भेद , रस, अलंकार, छन्द)
उत्तर-“कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम छन्द है।”
इस तरह काव्यशास्त्र के नियम के अनुसार, जिस कविता या काव्य में मात्रा, वर्ण, गण, यति, लय आदि का विचार करके शब्द योजना की जाती है, उसे छन्द कहते हैं।
उदाहरण-‘मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवठ सो दशरथ अजिर बिहारी॥
प्रश्न 2. निम्नलिखित के विषय में जानकारी दीजिए-
यति, लय, गति, तुक।
उत्तर-यति-छन्द का पाठ करते समय जहाँ थोड़ी देर रुका जाता है, उसे यति कहते हैं। लय-छन्द के पढ़ने की शैली को लय कहते हैं।
गति-गति का अर्थ है प्रवाह, अर्थात् छन्द को पढ़ते समय प्रवाह एक-सा हो।
तुक-पद के चरणों के अन्त में जो समान स्वर आते हैं तथा साम्य बैठाने के लिए लिये जाते हैं, उन्हें
तुक कहते हैं।
प्रश्न 3. छन्द के भेद बताइए और उनका परिचय दीजिए।
अथवा
मात्रिक छन्द व वर्णिक छन्द में क्या अन्तर है?
उत्तर-छन्द दो प्रकार के होते हैं-(1) वर्णिक छन्द, (2) मात्रिक छन्द।
(1) वर्णिक छन्द-वर्णिक छन्दों में वर्गों की गणना की जाती है तथा वर्णों की संख्या के आधार पर
छन्द का निर्धारण किया जाता है।
(2) मात्रिक छन्द-मात्रिक छन्दों में मात्राओं की गणना की जाती है।
नोट-दोहा एवं चौपाई मात्रिक छन्द हैं।
प्रश्न 4. छन्द किसे कहते हैं ? उसके कितने भेद हैं ? नाम लिखिए।
उत्तर-प्रश्न संख्या 1 तथा प्रश्न संख्या 3 के उत्तर देखिए।
प्रश्न 5. दोहा छन्द के लक्षण उदाहरण सहित समझाइए।
अथवा
दोहा छन्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए।
अथवा
दोहा छन्द के प्रत्येक चरण में कितनी-कितनी मात्राएँ होती हैं ?
उत्तर-दोहा-परिभाषा-दोहा छन्द के प्रथम और तृतीय चरणों में 13-13 और द्वितीय तथा चतुर्थ
चरणों में 11 – 11 मात्राएँ होती हैं। इसके सम चरणों के अन्त में तगण अथवा जगण का होना जरूरी है।
उदाहरण-
55|| 5513555।। 5113+11%D24
मेरी भव बाधा हरौ, राधा नागरि सोय।
5 II S SS IS SI 111 11 51 = 13 + 11 = 24
जा तन की झाँई परै, स्याम हरित दुति होय॥
प्रश्न 6. चौपाई छन्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए।
उत्तर-चौपाई-परिभाषा-चौपाई एक सममात्रिक छन्द है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएँ होती हैं।
उदाहरण-
SII || 15|| 55-16
मंगल भवन अमंगल हारी।
III III III 15 S = 16
द्रवउ सु दशरथ अजिर बिहारी॥
प्रश्न 7. दोहा छन्द की परिभाषा लिखिए तथा छन्द के प्रमुख अंगों के नाम बताइए।
उत्तर-दोहा छन्द की परिभाषा-कृपया प्रश्न 5 का उत्तर देखें।
छन्द के प्रमुख अंग-छन्द के छ: अंग होते हैं-(1) वर्ण, (2) मात्रा, (3) पाद या चरण, (4) यति,
(5) गति, और (6) तुक।
प्रश्न 8. गण के स्वरूप को समझाइए।
उत्तर-तीन वर्गों के समूह को गण कहते हैं। वार्णिक छन्दों में वर्ण की गणना की जाती है। उन वाणों
की लघुता और गुरुता के विचार के गणों के आठ रूप होते हैं।
प्रश्न 9. गणों के आठ रूप कौन-कौनसे होते हैं ?
उत्तर- गणों के आठ रूप और मात्राएँ इस प्रकार हैं-(1) यगण (155), (2) मगण (555), (3) तगण
(551),(4) रगण (5 । 5), (5) जगण (151), (6) भगण (511),(7) नगण (111),(8) सगण (115)
वस्तुनिष्ठ प्रश्न
• रिक्त स्थानों की पूर्ति
1. कविता के द्वारा सृष्टि के साथ मनुष्य के सम्बन्ध की रक्षा होती है। (रागात्मक/विवादात्मक)
2. अनुभूति के पक्ष का सम्बन्ध कविता के …………स्वरूप से है।
(बाहा/आन्तरिक)
3. मात्रिक छन्द का उदाहरण ……….” है।
(दोहा/सवैया)
4. ‘रस’ को काव्य की………………….बताया गया है।
(आत्मा/शरीर)
5. करुण रस का स्थायी भाव …………. है।
(शोक/करुणा)
6. वीर रस का स्थायी भाव…………………….(वत्सल/क्रोध)
7. रौद्र रस का स्थायी भाव…………………… है। (शोक/उत्साह)
8. खण्डकाव्य में जीवन का चित्रण होता है। (आंशिक/पूर्ण)
9. काव्य के……….. (दो/चार)
10. काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं। (अलंकार/रस)
उत्तर- 1. रागात्मक, 2. आन्तरिक, 3. दोहा, 4. आत्मा, 5. शोक, 6. उत्साह, 7. क्रोध, 8. आंशिक, 9.दो, 10. अलंकार।
•सही विकल्प चुनिए
भेद हैं।
1. शैली की दृष्टि से काव्य के भेद हैं-
(क) छः,
(ख) चार
(ग) दो,
(घ) तीन।
2. ‘कामायनी’ है-
(क) खण्डकाव्य, (ख) मुक्तक काव्य, (ग) महाकाव्य,(घ) इनमें से कोई नहीं।
3. हास्य रस का स्थायी भाव है-
(क) ह्यस,
(ख) उत्साह,
(ग) आश्चर्य,
(घ) सार्थक।
4. ‘रस’ के बिना काव्य माना जाता है-
(क) सजीव,
(ख) नीरस,
(ग) व्यर्थ,
(घ) शांत।
5. ‘बुन्देले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी।’
‘खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी।।’
इस पंक्ति में रस है-
(क) वीर,
(ख) करुण,
(ग) हास्य,
(घ) निर्वेद।
6. काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म (तत्व) कहलाते हैं-
अथवा
वे तत्व जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, कहलाते हैं-
(क) रस,
(ख) छन्द,
(ग) अलंकार,
(घ)काव्य गुण।
(घ) यमक अलंकार।
(घ)रूपक।
7. ‘चारु चन्द्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल-थल में’ में कौन-सा अलंकार है ?
(क) रूपक अलंकार,
(ख) अनुप्रास अलंकार,
(ग) श्लेष अलंकार,
8. ‘रघुपति राघव राजाराम’ में कौन-सा अलंकार है ?
(क) उपमा,
(ख) श्लेष,
(ग) अनुप्रास,
9. पीपर पात सरिस मन डोला’ में अलंकार है-
(क) उपमा,
(ख) रूपक,
(ग) उत्प्रेक्षा,
(घ) यमक।
10. जहाँ एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ होता है-
(क) अनुप्रास अलंकार, (ख) यमक अलंकार, (ग) श्लेष अलंकार,(घ) उपमा अलंकार।
उत्तर-1. (ग), 2. (ग), 3. (क), 4. (ख), 5. (क), 6. (ग), 7. (ख), 8. (ग), 9. (क), 10. (ग)।
सत्य/असत्य
1. तीन वर्गों के समूह को ‘गण’ कहते हैं।
2. वर्णिक छन्द में मात्राओं की गणना की जाती है।
3. प्रबन्ध काव्य में छन्दों में पूर्वापर सम्बन्ध नहीं होता।
4. छन्द तीन प्रकार के होते हैं।
5. मात्रिक छन्द में मात्राओं की गणना की जाती है।
6. शृंगार रस का स्थायी भाव रति है।
7. अलंकार का सामान्य अर्थ है-‘गहना’।
8. मुक्तक काव्य का प्रत्येक छन्द स्वतन्त्र होता है।
उत्तर-1.सत्य, 2. असत्य, 3. असत्य, 4. असत्य, 5. सत्य, 6. सत्य,7.सत्य,8. सत्य।
• एक शब्द/वाक्य में उत्तर
1. ‘चरण सरोज पखारन लागा’ में कौन-सा अलंकार है?
उत्तर-रूपक
2. एक ही छन्द में रचित एक घटना का चित्रण पूर्ण रूप से करने वाली रचना को क्या कहते हैं,
उत्तर-खण्डकाव्य।
3. रसात्मक वाक्य क्या कहलाता है ?
उत्तर-काव्य।
4. वीभत्स रस के स्थायी भाव का नाम क्या है?
उत्तर-जुगुप्सा (घृणा)।
5. हिन्दी काव्य साहित्य में रसों की संख्या कितनी मानी गई है?
उत्तर-नौ।
6. श्रृंगार रस के स्थायी भाव का नाम क्या है ?
उत्तर-रति (प्रेम)।
7. दोहा छन्द में कुल कितनी मात्राएँ होती हैं ?
उत्तर-481
8. काव्य के कितने भेद होते हैं ? नाम लिखिए।
उत्तर-काव्य के प्रमुख रूप से दो भेद-(1) दृश्य काव्य व (2) श्रव्य काव्य होते हैं।
9. विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं ?
उत्तर-महाकाव्य।
10. प्रबन्ध काव्य का एक भेद लिखिए।
उत्तर-महाकाव्य या खण्डकाव्य।

Leave a Reply